भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का विकास प्रारंभिक मध्यकालीन साहित्यिक इतिहास का महत्वपूर्ण भाग रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदी, पंजाबी, बंगाली और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषा ने उत्तर भारत में विकास किया तो तमिल, कन्नड़ और तेलुगु ने दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाई। इसी कड़ी में आइए जानते हैं साहित्य ने किस तरह क्षेत्रीय भाषाओं को अपने अंदर समाहित कर उन्हें एक नया जीवन दिया।
दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं
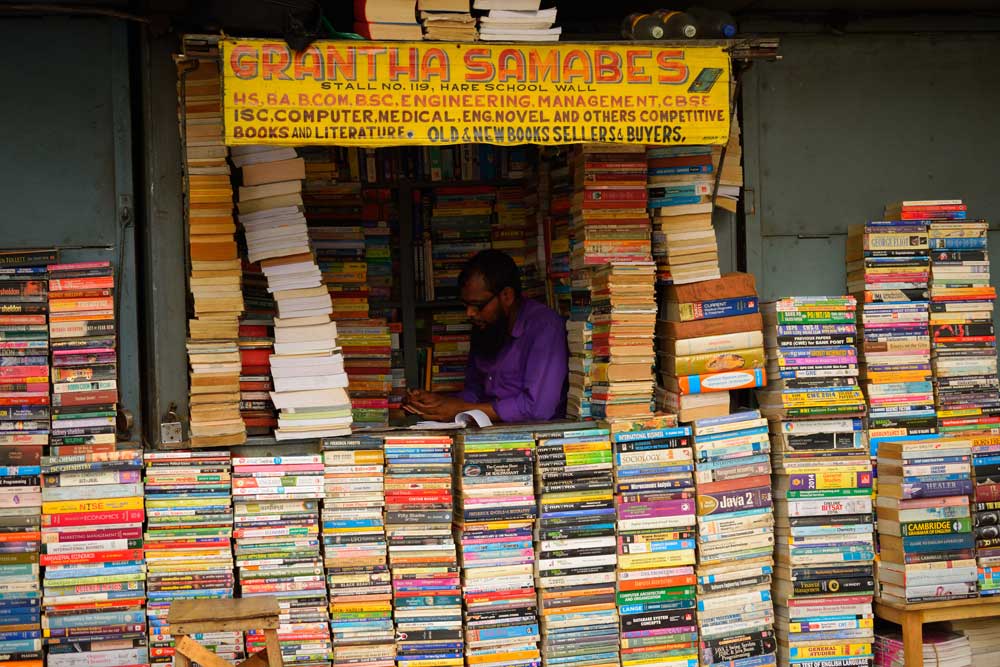
क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे पहले यदि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की चर्चा हम करें तो कन्नड़ और तेलुगु की तुलना में तमिल भाषा का साहित्यिक इतिहास काफी पुराना है, जिसकी शुरुआत ईसा युग से मानी जाती है। हालांकि इन तीनों के काफी समय बाद 14वीं सदी के आस-पास मलयालम भाषा का विकास हुआ। दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी इन क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा यदि हम उत्तर भारत की पहचान बन चुकी हिंदी की बात करें तो विद्वानों के अनुसार इसका विकास 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश से हुआ। इस काल को वीरगाथा काल या आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भक्ति काव्य के विकास से पहले वीरगाथा काल के अंतर्गत भाटों द्वारा लिखी गई कई क्षेत्रीय कविताएं आज भी उपलब्ध हैं। ये कविताएं विशेष रूप से विभिन्न राजपूत राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थी, जिनमें उनकी शक्ति और वीरता का बखान किया गया था।
खड़ी बोली हिंदी और हिंदवी की महाकाव्यात्मक रचनाएं
गौरतलब है कि साहित्य के अंतर्गत हिंदी की कई और किस्में भी रही हैं, जिनमें ब्रजभाषा, अवधि, राजस्थानी, मैथिलि, भोजपुरी और मालवी का समावेश था। इन भाषाओं के अलावा खड़ी बोली भी थी, जिसे कठोर, असभ्य और कच्ची बोली कहा जाता था। हालांकि अधिकतर मार्मिक कविताएं राजस्थानी में रची गईं, जिनमें पृथ्वीराज के प्रसिद्ध दरबारी मंत्री चंद बरदाई द्वारा लिखी गई ‘पृथ्वीराज रासो’ पहली और सबसे प्रसिद्ध कृति है। उसके बाद ‘विशालदेव रासो’, ‘हम्मीर रासो’, ‘खुमाना रासो’ और इसकी तरह कई और महाकाव्यात्मक रचनाएं हुईं। गौर करनेवाली बात ये भी है कि हिंदी साहित्य में सारी कविताएं प्रशंसात्मक नहीं थीं। इनमें बौद्ध सिद्धों और बाद में नागपंथी योगियों द्वारा लिखी गईं पवित्र कविताएं भी हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को न सिर्फ जन-जन तक पहुँचाया, बल्कि समृद्ध भी किया। इसके अलावा पश्चिमी भारत में जैन विद्वानों द्वारा राजस्थानी में रची गईं धार्मिक कविताओं में लोगों के सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर ज़ोर दिया गया। ये रचनाएं, हिंदी की बजाय हिंदवी कहलाई।
7वीं शताब्दी से शुरू हुआ संकलन और संग्रहण का काम
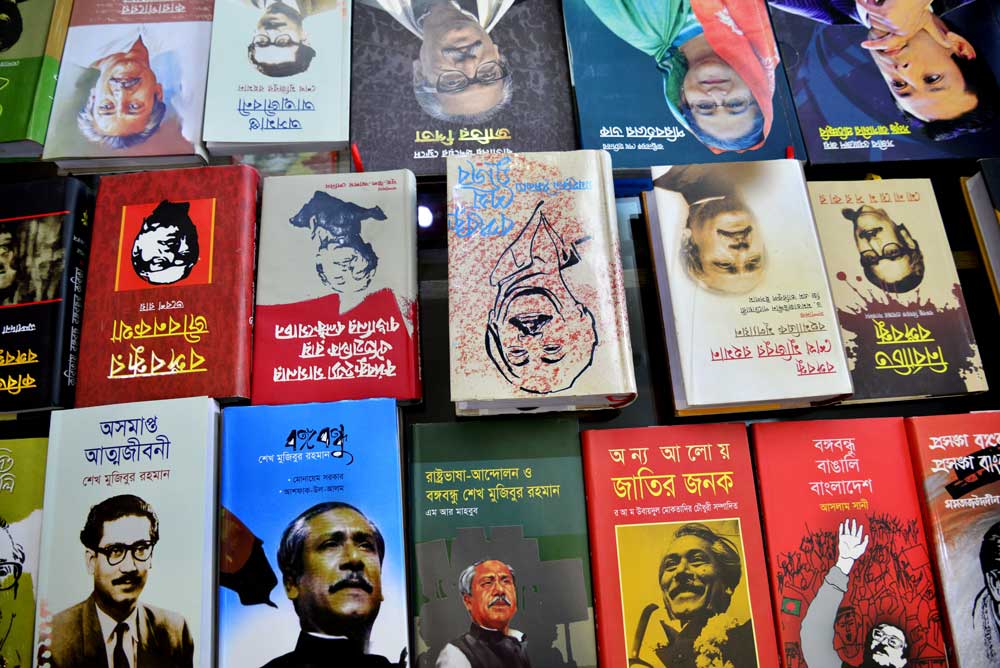
जैसा कि अभी हमने बताया भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का विकास प्रारंभिक मध्यकालीन साहित्यिक इतिहास का महत्वपूर्ण भाग रहा है, और ये छठी शताब्दी में शुरू हुए भक्ति प्रेरित साहित्यिक आंदोलनों का परिणाम थे। इनमें विशेष रूप से पल्लव और पांड्य राजाओं के संरक्षण में रहनेवाले नयनार और अलवर नामक कवियों द्वारा शिव और विष्णु के सम्मान में रचे गए भजनों का समावेश होता है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले इन भजनों की रचना 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुई थी, जो आज भी संग्रहित है। इन भजनों को संग्रहित करने की वजह ये भी थी कि आगामी शताब्दियों में लगातार नए भजनों की रचना हो रही थी और उन्हें संकलित किया जा रहा था। इस तरह 780 ईस्वी से 830 ईस्वी के बीच संकलनकर्ता सुनतार ने पहला संकलन बनाया, जिसमें 62 नयनार कविताएं शामिल हुईं। हालांकि बाद में रचे गए भजनों को 11वीं शताब्दी में नम्पी अंतर नम्पी ने संकलित की। 11वीं शताब्दी से पहले ही 10वीं शताब्दी में नटमुनि ने नालयीरतिव्य पापदम नामक वैष्णव धर्मग्रंथ का संकलन किया, जिसमें 14 कवियों द्वारा लिखे गए 4000 भजन थे। इन 4000 भजनों में 12 अलवर थे।
चोल राजा और उनके दरबारी कवियों के साथ कंपन की श्रेष्ठता
विशेष रूप से तमिल साहित्य के साहित्यिक विकास की बात करें, तो इसका श्रेय चोल राजवंश को जाता है। चोल राजवंश में स्तुति लेखन की दो विधाएँ, पराणी और उला शुरू हुई थीं, जिनमें पराणी के अंतर्गत सैन्य कारनामों और उला के अंतर्गत राजा द्वारा शहर भ्रमण का उल्लेख किया गया है। पराणी के अंतर्गत चोल राजा कुलोत्तुंग के दरबारी कवि जयमागोंडा ने कलिंगाट्टुपरानी नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में राजा के कलिंग युद्ध अभियान के वर्णन के साथ उनकी युद्ध रणनीतियों का बखान किया गया है। हालांकि उला विधा का श्रेय विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराजा द्वितीय के दरबारी कवि ओट्टुकुटार को जाता है। चोल कवियों द्वारा रचे गए इन प्रशंसात्मक रचनाओं से इतर प्रसिद्ध चोल कवि कंपन ने रामायण का तमिल संस्करण ‘राम-अवतारम’ लिखा था, जिसकी भाषा उत्कृष्ट होने के साथ-साथ गीतात्मक और भावपूर्ण भी थी। इस रचना के फलस्वरूप ‘कविचक्रवर्ती’ की उपाधि से सम्मानित कंपन ने रामायण से सीधा अनुवाद करने की बजाय इसमें रामायण की कई घटनाओं की पुनर्व्याख्याएँ भी की हैं, जो बेजोड़ हैं।
शासकों के साथ कवियों ने समृद्ध की कन्नड़ भाषा
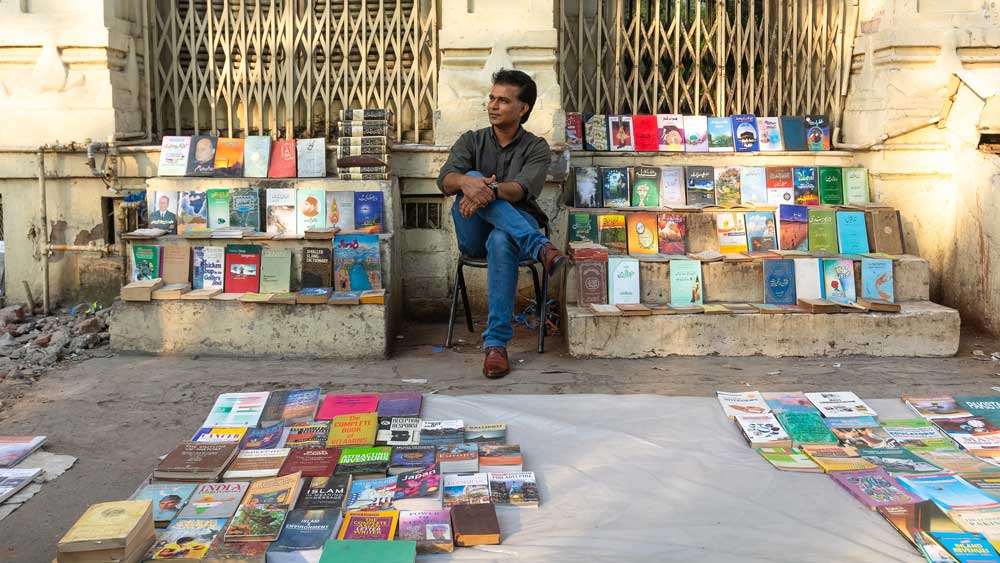
दक्षिण में क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत कन्नड़ भाषा का उपयोग 5वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था, लेकिन इसका विकास राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रकूट शासकों ने ही क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन देना शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप कन्नड़ की पहली महत्वपूर्ण कृति कविराजमार्ग की रचना हुई। हालांकि कुछ विद्वान इसका श्रेय राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को देते हैं, तो कुछ उनके दरबारी कवि श्रीविजय को देते हैं, जिन्होंने इसे लिखा था। इस पुस्तक में कन्नड़ भाषा और साहित्यिक परंपराओं पर चर्चा की गई है, जिसे 527 श्लोकों के साथ 3 अध्यायों में समेटा गया है। सिर्फ यही नहीं इसमें कन्नड़ और संस्कृत के मिश्रण के नियमों के साथ ध्वनि संयोजन को शामिल किया गया है, जो आज भी कन्नड़ कवियों के लिए एक आधारभूत कृति है। श्रीविजय के बाद कन्नड़ साहित्य में पंपा, पोन्ना और रन्न नामक तीन उत्कृष्ट कवि हुए, जिन्होंने क्षेत्रीय साहित्यिक आंदोलन को और प्रभावित किया। इन्होने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से महाभारत के साथ जैन धर्म पर भी चर्चा की। ये तीनों कवि राष्ट्रकूट शासकों के दरबारी कवि थे, लेकिन अपनी रचनाओं से इन्होने कन्नड़ साहित्य की दशा ही नहीं, दिशा भी बदल दी।
तेलुगु साहित्यिक रचनाएं और उनकी आधारशिला
क्षेत्रीय भाषाओं में तेलुगु की बात करें तो तेलुगु का उपयोग 6ठी शताब्दी की शुरुआत से अधिकतर शिलालेखों में किया जाता रहा है। हालांकि इसके अंतर्गत पहली रचना प्रारंभिक मध्यकाल में रची गई थी। फिलहाल तेलुगु साहित्य का शुरुआती अंश आज भी महाभारत के आदि और सभा पर्व में मौजूद हैं, जिनका अनुवाद कवि नन्नया ने किया था और इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। कन्नड़ कवियों की तरह ही तेलुगु कवियों ने भी महाभारत के कई अतिरिक्त अनुवाद किए, जिनमें विराट पर्व और वन पर्व प्रमुख है। इसकी रचना तेलुगु के सुविख्यात कवि टिक्कना और येर्राप्रगदा ने किया था। उनकी रचनाओं ने तेलुगु साहित्य को मजबूत बनाने में आधारशिला का काम किया था। हालांकि 13वीं शताब्दी में बुद्धराज ने भी रामायण महाकाव्य का अनुवाद किया, लेकिन वे वाल्मीकि द्वारा रचे गए संस्कृत रामायण का महज अनुवाद था। गौरतलब है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच सामंती विकास के कारण क्षेत्रीय संस्कृतियां निर्मित हुईं, जिनके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारतीय शासकों ने जहां कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा को प्रोत्साहित किया, वहीं उत्तर भारत में अकबर के शासनकाल में फारसी, गुजराती और राजस्थानी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं साहित्यिक रूप से समृद्ध हुईं। दिलचस्प बात ये है कि क्षेत्रीय भाषाओं को और मजबूत करने में स्थानीय और क्षेत्रीय सुल्तानों का भी काफी योगदान रहा है।
Lead image courtesy: @sabrangindia.in