हिंदी साहित्य में शृंगार रस का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो मानवीय प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। शृंगार रस मुख्यतः प्रेम और श्रृंगार अर्थात सौंदर्य पर आधारित होता है। आइए जानते हैं हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस।
रीतिकाल के अलावा आदिकाल में भी रहा श्रृंगार रस का बोलबाला
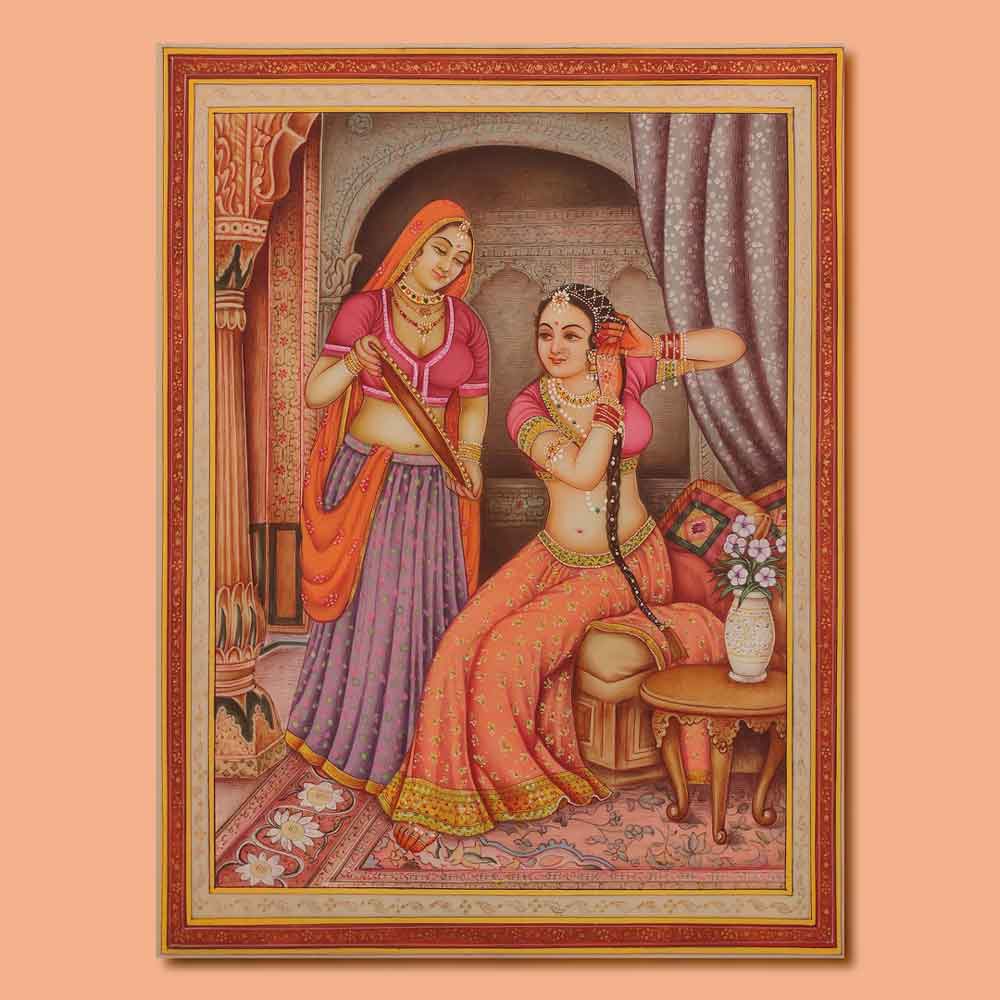
Picture Courtesy: @etsy.com
हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का समावेश है। आदिकालीन साहित्य में मुख्यतः वीर रस की प्रधानता है, लेकिन यहाँ धर्म, नीति और श्रृंगार आदि से सम्बंधित साहित्य भी उपलब्ध हैं। भक्तिकाल में मुख्यतः भक्तिपरक काव्य की प्रधानता रही है, जिनमें संतकाव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्णभक्ति काव्यधारा और रामभक्ति काव्यधारा हैं, लेकिन आदिकाल के कवि 'विद्यापति' की रचना 'पदावली' के दोहों में 'श्रृंगार समन्वित भक्ति' के पद भी हैं।। हालांकि भक्तिकाल के बाद आनेवाले रीतिकाल में भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया। गौरतलब है कि रीतिकालीन काव्यों में श्रृंगार प्रधान होने के बावजूद वीरता, भक्ति और नीति से सम्बंधित साहित्य भी उपलब्ध है।
साहित्य में श्रृंगार रस है स्थायी भाव
जिस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, उसी प्रकार काव्य को पढ़ने के बाद पाठक के मन में आनंद की जो अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने की अवस्था ही 'रस' कहलाती है। जिस प्रकार अलंकार काव्य का आभूषण है, उसी प्रकार रस काव्य की आत्मा है। रस के चार प्रकार हैं - स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। साहित्य में स्थाई भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसा स्थाई भाव होगा वैसा ही रस होगा। सर्वप्रथम भरत मुनि ने 'नाट्यशास्त्र' में स्थाई भावों की संख्या 8 मानी थी लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान रसों की संख्या 9 मानते हैं तो कुछ 10 तो कुछ विद्वान 11 भी मानते हैं।
बिहारी के दोहों में संयोग श्रृंगार रस
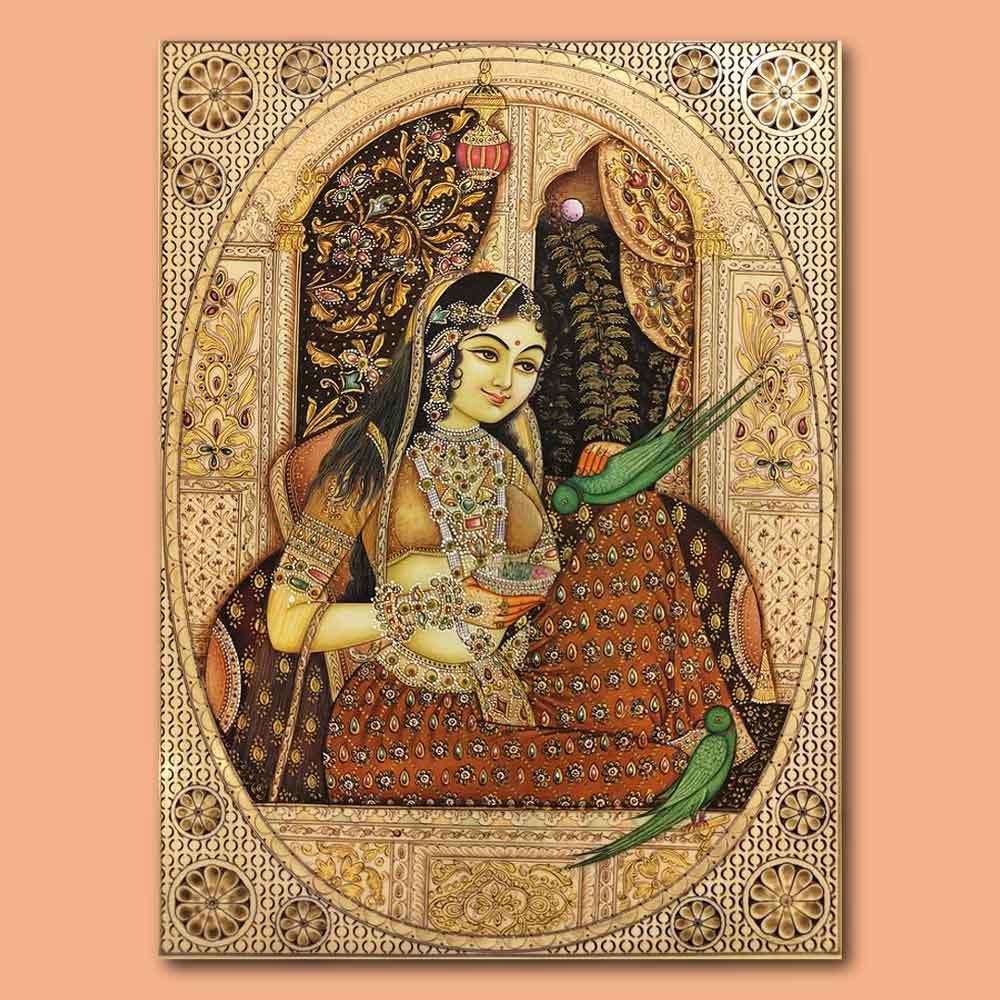
Picture Courtesy: @pixels.com
श्रृंगार रस को 'रसों का राजा' माना गया है। इसकी उत्पत्ति के लिए स्थाई भाव 'रति' जिम्मेदार है। यह रस दो प्रकार का होता है- संयोग और वियोग। सरल शब्दों में कहें तो संयोग श्रृंगार में नायक-नायिका के परस्पर मिलन कि अनुभूति होती है, जबकि वियोग में नायक- नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन उनके मिलन का अभाव होता है। संक्षेप में कहें तो संयोग में मिलन की अनुभूति होती है तो वियोग में विरह की। संयोग श्रृंगार रस के लिए हिंदी साहित्य में सबसे विख्यात हैं रीतिकाल के कवि बिहारी। बिहारी के कुछ दोहों को पढ़ने मात्र से चलचित्र देख लेने जैसा अनुभव पाठक को प्राप्त होता है। प्रस्तुत हैं बिहारी के श्रृंगार रस से परिपूर्ण कुछ दोहे -
"बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।
सौंह करै भौंहनु हँसे , दैन कहै , नटि जाय।।"
"कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात।
भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सों बात॥"
"पतरा ही तिथी पाइये, वा घर के चहुँ पास।
नित प्रति पून्यौई रहे, आनन-ओप उजास॥"
"अंग अंग नग जगमगत दीपसिखा सी देह।
दिया बुझाय ह्वै रहौ, बड़ो उजेरो गेह॥"
"तंत्रीनाद, कवित्त-रस, सरस राग, रति-रंग।
अनबूड़े बूड़े , तिरे जे बूड़े सब अंग।।"
श्रृंगार के जरिए आडंबरों पर भी चोट करते हैं बिहारी
आम तौर पर बिहारी के काव्यों को पूर्णतः सामंती मानसिकता से परिपूर्ण श्रृंगारपरक क्रीड़ा और भोग प्रधान माना जाता रहा है, लेकिन सच पूछिए तो ऐसा नहीं है। बिहारी के दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ सामाजिक चेतना भी मौजूद है। राजनीतिक चेतना की उपस्थिति के साथ वे धार्मिक अंधविश्वास पर चोट और पारिवारिक समन्वय भी दर्शाते हैं। उदाहण के तौर पर धर्म के क्षेत्र में प्रचलित आडंबरों पर चोट करते हुए बिहारी लिखते हैं -
"जप माला छापै तिलक, सैर न एकौ काम।
मन काँचे नाचै बृथा, साचै राँचे राम ।।"
जायसी और सूरदास के दोहों में वियोग श्रृंगार रस

Picture Courtesy: @2.bp.blogspot.com
यदि हम वियोग श्रृंगार रस की बात करें तो हम पाते हैं कि सूरदास के भ्रमरगीत सार के साथ जायसी के 'पद्मावत' में भी इसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत हैं कुछ उदाहरण-
जायसी के पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन -
“पिय सौं कहेहु सँदेसरा हे भौंरा! हे काग!!
सो धनि बिरहै जरि मुइ तेहिक धुवाँ हमहि लाग।।”
“बरसै मघा झकोरी झकोरी।
मोर दुइ नैन चुवै जस ओरी।।”
“फिरि फिरि रोव, कोइ नहीं डोला । आधी राति बिहंगम बोला ॥
"तू फिरि फिरि दाहै सब पाँखी । केहि दुख रैनि न लावसि आँखी"
सूरदास के भ्रमरगीत सार से -
"निसिदिन बरसत नैन हमारे।
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते स्याम सिधारे।।"
"अंखियां हरि-दरसन की भूखी।
कैसे रहैं रूप-रस रांची ये बतियां सुनि रूखी॥
अवधि गनत इकटक मग जोवत तब ये तौ नहिं झूखी।
अब इन जोग संदेसनि ऊधो, अति अकुलानी दूखी॥
बारक वह मुख फेरि दिखावहुदुहि पय पिवत पतूखी।
सूर, जोग जनि नाव चलावहु ये सरिता हैं सूखी॥"
"अति मलीन वृषभानुकुमारी।
हरि स्त्रम जल भीज्यौ उर अंचल, तिहिं लालच न धुवावति सारी।।
अध मुख रहति अनत नहिं चितवति, ज्यौ गथ हारे थकित जुवारी।
छूटे चिकुरे बदन कुम्हिलाने, ज्यौ नलिनी हिमकर की मारी।।
हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भइ, इक विरहिनि, दूजे अलि जारी।
‘सूरदास’ कैसै करि जीवै, व्रजवनिता बिन स्याम दुखारी॥"
"मधुवन तुम कत रहत हरे।
विरह-वियोग स्याम सुन्दर के ठाढे क्यौं न जरे॥"
छायावादी कवियों का श्रृंगार वर्णन
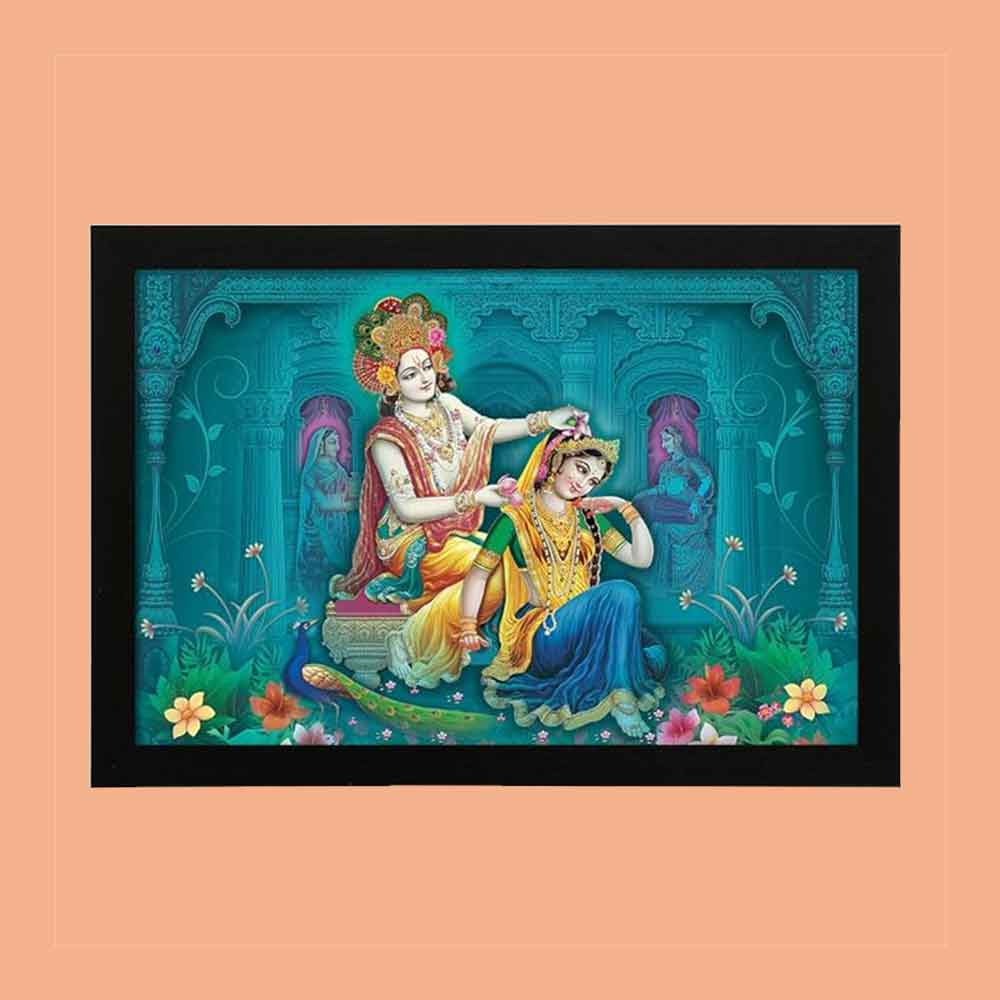
Picture Courtesy: @amazone.in
रीतिकालीन काव्यों के अलावा, छायावाद में भी कई स्थानों पर श्रृंगार रस उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत है छायावादी कवियों द्वारा श्रृंगार रस की प्रधानता के कुछ उदाहरण -
छायावाद में सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं -
"वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।
निकलकर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान."
छायावाद में ही महादेवी वर्मा लिखती हैं -
"कौन आया था न जाना
स्वप्न में मुझको जगाने;
याद में उन अँगुलियों के
है मुझे पर युग बिताने;
रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ !
शून्य मेरा जन्म था
अवसान है मूझको सबेरा;
प्राण आकुल के लिए
संगी मिला केवल अँधेरा;
मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ !"
नायक और नायिका के साथ प्रकृति चित्रण भी है महत्वपूर्ण
हिंदी साहित्य में आदिकाल में विद्यापति से ही श्रृंगार वर्णन की परंपरा चली आ रही है, जो आज तक जारी है, किंतु साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर बिहारी का श्रृंगार वर्णन पाठकों की प्रिय पसंद रही है। इसकी वजह है छोटे छंदों में भी अनुभावों की सघनता से श्रृंगार वर्णन को बिंबात्मक और सजीव बना देना। यही वजह है कि उनके दोहों के लिए कहा भी गया है कि "सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर॥" शृंगार रस में प्रेम, खुशी, उत्साह, उदासी, और दर्द जैसी भावनाओं की गहन अभिव्यक्ति होती है, जिसे शब्दों और छंदों के साथ अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण बनाया जाता है, जो पाठक को आनंदित करता है। नायक और नायिका के रूप, गुण, और आचरण के वर्णन के साथ प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रकृति का चित्रण किया जाता है, जैसे बगीचे, पुष्प, नदी, चंद्रमा, और वसंत ऋतु।
आध्यात्मिक प्रेम से सराबोर श्रृंगार रस
शृंगार रस केवल प्रेम का वर्णन नहीं करता, बल्कि मनुष्य की भावनाओं, संबंधों और संवेदनाओं की गहराई को उजागर करता है। यह रस पाठक को मानसिक और भावनात्मक आनंद प्रदान करता है और जीवन के सुंदर पहलुओं को सजीव बनाता है। यही वजह है कि शृंगार रस को साहित्य का सम्पूर्ण रस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार रस के अंतर्गत अपने प्रियतम के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है, किंतु ऐसा नहीं है। यह रस केवल नायक-नायिका के प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मातृ-प्रेम, भक्त-प्रेम, और मानवीय प्रेम का भी चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक प्रेम के अंतर्गत एक तरफ जहां आप कृष्ण और मीरा का प्रेम पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सूरदास और कृष्ण, तुलसीदास और राम का प्रेम दर्शाया गया है। गौरतलब है कि महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में जहाँ श्रृंगार रास के संयोग और वियोग को दर्शाया है, वहीं तुलसीदास ने सीता विरह को राम के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया है।
Lead Picture Courtesy: @amazone.in